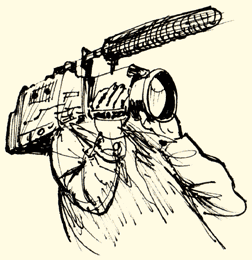 डौक्यूमेण्ट्री शब्द से यही मालूम देता है कि इसका सम्बन्ध डौक्यूमेण्ट करने या किसी भी घटना की एक स्मृति, एक यादगार तैयार करने से है। मूलतः यह बात सही है। गतिमान चित्रों की सबसे पहली फ़िल्म, लूमियर बन्धु द्वारा बनाई गई ‘स्टेशन पर ट्रेन का आगमन’ वास्तव में एक डौक्यूमेण्ट्री ही थी। ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी, फ़िल्मकार ने उसे कैमरा लगा के एक यादगार के रूप में क़ैद कर लिया। लेकिन बाद के वर्षों में गतिमान चित्रों की इस कला का वह स्वरूप अधिक लोकप्रिय हुआ जिसे हम सिनेमा के नाम से जानते हैं, जिस में एक वास्तविकता से मिलती-जुलती एक कहानी होती है, पेशेवर अभिनेता होते हैं, विस्मयकारी दृश्य होते हैं, और जिसे नाटकों की तरह मंचित किया जाता है। चूंकि लगभग सौ वर्षों तक गतिमान चित्रों की यह कला बेहद महँगी टेक्नोलौजी पर आधारित थी इसलिए डौक्यूमेण्ट्री के रूप में फ़िल्म का प्रयोग बेहद सीमित रहा। आम जन अपने आम जीवन की घटनाओं को स्थायी स्मृतियों में बदलने के लिए इस कला का व्यवहार नहीं कर सके।
डौक्यूमेण्ट्री शब्द से यही मालूम देता है कि इसका सम्बन्ध डौक्यूमेण्ट करने या किसी भी घटना की एक स्मृति, एक यादगार तैयार करने से है। मूलतः यह बात सही है। गतिमान चित्रों की सबसे पहली फ़िल्म, लूमियर बन्धु द्वारा बनाई गई ‘स्टेशन पर ट्रेन का आगमन’ वास्तव में एक डौक्यूमेण्ट्री ही थी। ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी, फ़िल्मकार ने उसे कैमरा लगा के एक यादगार के रूप में क़ैद कर लिया। लेकिन बाद के वर्षों में गतिमान चित्रों की इस कला का वह स्वरूप अधिक लोकप्रिय हुआ जिसे हम सिनेमा के नाम से जानते हैं, जिस में एक वास्तविकता से मिलती-जुलती एक कहानी होती है, पेशेवर अभिनेता होते हैं, विस्मयकारी दृश्य होते हैं, और जिसे नाटकों की तरह मंचित किया जाता है। चूंकि लगभग सौ वर्षों तक गतिमान चित्रों की यह कला बेहद महँगी टेक्नोलौजी पर आधारित थी इसलिए डौक्यूमेण्ट्री के रूप में फ़िल्म का प्रयोग बेहद सीमित रहा। आम जन अपने आम जीवन की घटनाओं को स्थायी स्मृतियों में बदलने के लिए इस कला का व्यवहार नहीं कर सके। अन्य देशों की तरह भारत में सबसे पहले डौक्यूमेण्टरी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण घटनाओं को दस्तावेज़ के रूप बन्द करने के लिए अंग्रेज़ों ने किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अपने पक्ष का सम्बल बनाए रखने के लिए उन्होने एक प्रकोष्ठ भी बनाया लेकिन उसके पहले से ही अपनी प्रजा को समझने की औपनिवेशिक मानसिकता से हैन्स नीटर के ‘ए रोड इन इण्डिया’ जैसी लघुफ़िल्में भी बनती रही थीं।
विस्मयकारी अनोखे नज़ारों और ऐतिहासिक घटनाओं की राह से निकल कर फ़िल्म इतिहास में बहुत जल्दी ही डौक्यूमेन्टरी का शब्द राजनैतिक प्रचार की फ़िल्मों के अर्थ में रूढ़ हो गया और इस प्रक्रिया में नाज़ी समर्थक जर्मन फ़िल्मकार लेनी राफ़ेन्स्थाल की मुख्य भूमिका सी रही। उनके फ़िल्मों के भीतर के नाज़ी तत्व को तो लोगों ने नकार दिया मगर फ़िल्म माध्यम का इस्तेमाल प्रचार के लिए कैसे किया जाय, ये उनसे सीख लिया। यह प्रयोग आज़ादी के पहले अंग्रेज़ो ने अपने हितों के लिए किया फिर स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी उसे जारी रखा।
देश के आज़ादी के बाद नेहरू जी सिनेमा की ताक़त को समझ कर फ़िल्म्स डिवीज़न की नींव डाली जिन्हे हर हफ़्ते एक वृत्तचित्र बनाने की बन्दिश थी। भारतीय जनमानस में डौक्यूमेण्ट्री की पूर्वतम स्मृति के रूप में क़ैद ये वृत्त चित्र फ़ीचर फ़िल्मों के पहले दिखलाया नियमबद्ध था। इनका मक़्सद तो नेहरू की नीतियों व नवोदित भारतीय राज्य के राजनीतिक आदर्शों का प्रचार ही था मगर अपनी सीमाओं के भीतर ही फ़िल्म्स डिवीज़न में प्रमोदपति, सुखदेव और एस एन एस शास्त्री जैसे लोगों ने डौक्यूमेण्टरी का एक कलारूप के बतौर ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। उनकी फ़िल्में आई एम ट्वेन्टी या इण्डिया सिक्सटी सेवेन आज भी याद की जाती हैं। मणि कौल व कुमार साहनी ने फ़िल्म्स डिवीज़न के लिए जो फ़िल्में बनाईं वो इसी कलात्मक परम्परा में थीं। लेकिन ये सभी फ़िल्में राज्य, उसके चरित्र और उसकी गतिविधि पर ही केन्दित हो कर उसका प्रचार करती रहीं।
सत्तर के दशक में जब इंदिरा गांधी की तानाशाही के ख़िलाफ़ और इमरजेन्सी के आस-पास जो प्रतिरोध की राजनीति पनपी का उसकी एक अभिव्यक्ति प्रतिरोध की डौक्यूमेण्टरी, या भूमिगत डौक्यूमेण्टरीज़ में हुई। इस अभिव्यक्ति का परचम आनन्द पटवर्धन के हाथ में लहरा रहा था। आने वाले दो दशकों तक वे न सिर्फ़ डौक्यूमेण्टरी के शिखर पुरुष बने रहे बल्कि राजनैतिक नैतिकता व आदर्श की चरम अभिव्यक्ति भी।
ऐनालौग वीडियो तकनीक के आ जाने से अस्सी के दशक में ही एक बड़े परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरु हो गई थी जो नब्बे के दशक में डिजिटल के विस्फोट से एक क्रांति में बदल गई। हाई-ऐट और ऐविड जैसे नए माध्यमों के आने से वीडियो पहले से कहीं अधिक सुलभ और सरल हो गया। और दूसरी तरफ़ देश में उदारीकरण की नीतियों के चलते देश में संचार क्रांति हो गई। 90 के दशक के बाद और ख़ासकर नई सदी में डॉक्यमेंट्री फिल्मों की ओर आकर्षण बढ़ा है, लेकिन अब भी यह इतना नहीं है कि पश्चिम की डॉक्यमेंट्री विधा के सामने खड़ा हो सके। स्वाभाविक है कि इसका कोई एक कारण नहीं है। हाल के वर्षों में ज़रूर मास कम्यूनिकेशन संस्थानों में प्रशिक्षण और प्रदर्शन के नए तरीक़ों के आने के बाद डौक्यूमेण्ट्री की लोकप्रियता में पहले के मुका़बले इज़ाफ़ा हुआ है।
***
इस पूरे बदलाव पर बातचीत करते हुए आज के डौक्यूमेण्ट्री परिदृश्य में अपनी एक सशक्त पहचान बना चुकीं पारोमिता वोहरा कहती हैं कि भारत में सरकारी तंत्र के बाहर डौक्यूमेण्ट्री फ़िल्मों के लिए कोई ठोस वित्तीय सहायता न होने के कारण शुरुआती दौर में अधिकतर फ़िल्में राजनैतिक आन्दोलनों के संसर्ग में ही बनीं; और ये भी कहना अनुचित नहीं होगा कि वे उन आन्दोलनों के द्वारा ही प्रायोजित थीं। १९९० के पहले या तो फ़िल्में सरकारी तत्वाधान में बन रही थीं या राजनैतिक आन्दोलनों के तत्वाधान में।
भारत में डौक्यूमेण्ट्री के इतिहास की समझ को एक दिलचस्प लोच देती हैं मुम्बई स्थित सांस्कृतिक संस्था ‘मजलिस’ की संचालक और स्वतंत्र डौक्यूमेण्ट्री फ़िल्मकार मधुश्री दत्ता; वे कहती हैं कि भारत में डौक्यूमेण्ट्री की शुरुआत राज्य की तरफ़ से ही हुई और जब सत्तर के दशक में जब आनन्द पटवर्धन जैसे फ़िल्मकारों ने ‘प्रिज़नर्स औफ़ कान्शसनेस’ जैसी प्रतिरोध की डौक्यूमेण्ट्री बनाना आरम्भ किया तो उनका भी ध्यान पूरी तरह से राज्य पर ही केन्द्रित रहा। वे राज्य के यथार्थ के एक दूसरे पहलू का उद्घाटन करते रहे।
९० के बाद आने वाले बड़े बदलाव के पहले ८० के दशक में एक छोटा बदलाव भी आता है। एक तरफ़ तो फ़िल्म के सिल्वर आयोडाइड के बदले वीडियो के प्रचलन से टेक्नोलौजी ने करवट बदली और दूसरी तरफ़ उत्तर आधुनिकता, इतिहास के वैकल्पिक चिन्तन, और नारीवाद जैसे आन्दोलनों के चलते यथार्थ को देखने की एक नई दृष्टि का भी विकास हुआ। एक तरफ़ यथार्थ को कैमरे में क़ैद करने की नई बहुसुलभ तकनीक विकसित हो रही थी और दूसरी यथार्थ को समझने की नई नज़र भी विकसित हो रही थी। मधुश्री मानती हैं कि ९० के दशक में पनपा डौक्यूमेण्ट्री का कलारूप इन दो परिघटनाओं के संयोग का परिणाम है। क्योंकि रीनामोहन द्वारा बनाई गई फ़िल्म ‘कमलाबाई’ (१९९२) जो हिन्दी सिनेमा की प्रथम महिला कलाकार के निजत्व से निकट से रूबरू कराती है, १६एमएम पर ज़रूर बनाई गई लेकिन उसका सौन्दर्यबोध और यथार्थबोध उस नए चिंतन से प्रभावित है जिसने बाद के वर्षो में डौक्यूमेण्ट्री के कई कलारूपों को जन्म दिया।
लेकिन यह समझ लेना कि डौक्यूमेण्ट्री कोई प्रगतिशील माध्यम है, सही न होगा। डौक्यूमेण्ट्री भी किसी भी कलारूप की तरह है जिसका चरित्र उसके इस्तेमाल करने वाले की समझ व नैतिकता से प्रभावित हो कर बदलता रहता है। पारोमिता कहती हैं कि शुरुआत में अधिकतर फ़िल्में वाम-लोकतांत्रिक शक्तियों के पक्ष में बनीं लेकिन बाद में राम जन्म भूमि आन्दोलन के अन्तर्गत ‘भए प्रगट कृपाला’ जैसी फ़िल्मों का भी निर्माण हुआ जिनके द्वारा विकसित शैली का इस्तेमाल आज भी कई हिन्दी समाचार चैनल करते आ रहे हैं।
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फ़िल्मकार और मूर्धन्य चिंतक कमल स्वरूप के अनुसार हाथ में छिप से जाने वाले डीवी कैमरों के आने से सब से बड़ा बदलाव ये आया कि फ़िल्म बनाने वाले और फ़िल्म पर नज़र आने वाले आदमी के बीच यंत्र का महत्व भी घट कर बेहद मामूली हो गया। उनका कहना है कि आज डौक्यूमेण्ट्री के मंज़र में जो बाढ़ आई है उसके केन्द्र में यह सर्वसुलभ टेक्नोलौजी ही है, सस्ते कैमरे आने से सब के हाथ में कैमरा आ गया। वरना कैमरा एक ऐसा बहुईष्यित यंत्र था जिस का स्पर्श कुछ कुलीनजन ही कर सकते थे। पारोमिता वोहरा के अनुसार १९९० के बाद हुए टेक्नोलाजिकल बदलाव का सबसे बड़ा असर यह रहा कि सस्ते कैमरे और सस्ती सम्पादन मशीनों के चलते फ़िल्मकार अपने उत्पादन के साधनों का मालिक ख़ुद होने लगा।
पारोमिता यह भी मानती हैं कि भारत में १९९० में एक बड़ा राजनैतिक-आर्थिक परिवर्तन आया, और इन बदली हुई राजनीतिक सच्चाईयां में ७० व ८० के दशक का डौक्यूमेण्ट्री कलारूप पर्याप्त नहीं रह गया था। आज का युवा अपना जीवन कई स्तर पर जी रहा है, और इसीलिए डौक्यूमेण्ट्री में भी एक ऐसे कलारूप की तलाश शुरु हुई जो अपने आस-पास की सच्चाई को उसकी पूरी जटिलता में पकड़ सके। बदल गईं। पहले वाले कलारूप नकारे नहीं गए, लेकिन और नए कलारूपों का प्रयोग किया जाने लगा।
प्रतिष्ठित डौक्यूमेण्ट्री फ़िल्मकार और एफ़ टी आई आई, पुणे में निर्देशन के प्राध्यापक अजय रैना इसे तो मानते हैं कि पिछले बीस सालों में डौक्यूमेण्ट्री के परिदृश्य में पुरानी प्रचारवादी फ़िल्मों से इतर निजी जीवन पर केन्दित, काव्यात्मक और अमूर्त शैलियों का विकास हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि योरोप व अमरीका में ये कलारूप पहले से ही विकसित हो चुके थे। डिजिटल तकनीक की सुलभता के कारण ही इस तरह के कलाप्रयोग भारत जैसे ग़रीब देश में भी मुमकिन हो सके।
धीरे-धीरे ‘सत्य के पर्दाफ़ाश’ वाली डौक्यूमेण्टरी, और ‘सत्य के प्रचार’ वाली सोच की विरासत न्यूज़ चैनलों ने सम्हाल ली, हालांकि यह कहा जा सकता है कि वो सत्ता पक्ष के ‘सत्य’ को ही प्रचारित करते रहे और ‘जनता’ के पक्ष के प्रचार की जगह बनी रही और इसीलिए डौक्यूमेण्ट्री की प्रचार शैली पूरी तरह से विलीन नहीं हुई। कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन पर ‘जश्ने आज़ादी’ (२००७) और नर्मदा के सरदार सरोवर डैम के विरुद्ध चल रहे जनान्दोलन पर ‘वर्ड्स औन वाटर’ (२००३) फ़िल्म बनाने वाले संजय काक जैसे क्रोधित फ़िल्मकार भारतीय राज्य के चरित्र को नंगा करते हुए अभी तक भू-भ्रमण कर रहे हैं। पर शायद यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि डौक्यूमेण्ट्री की प्रचारशैली अब ओल्ड-फ़ैशण्ड हो चली है।
***
पहले से स्थापित डौक्यूमेण्ट्री के रहस्योद्घाटक क़िस्म के स्वरूप को नए फ़िल्मकारों ने चुनौती दी। मधुश्री मानती हैं कि ये नए फ़िल्मकार यथार्थ का अनावरण करके उसे अपनी विचारधारा के पक्ष में सबूत की तरह पेश नहीं करते, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर निलिता वछानी की फ़िल्म ‘आईज़ औफ़ स्टोन’ (१९९०) जो एक राजस्थानी औरत शांता की कहानी है जिस पर ‘माता’ आती हैं। फ़िल्म न तो इस परम्परा पर कोई निर्णय सुनाती हैं और न ही इसे कोई सैद्धान्तिक चोला पहनाती है। वे दर्शक को कोई संदेश नहीं देती बल्कि इस अवधारणा को सोचने-समझने की प्रक्रिया में दर्शक को हिस्सेदार कर लेती है। डौक्यूमेण्ट्री के इतिहास में इस शैली को सिनेमा वेरिते (सच्चा सिनेमा) के नाम से जाना गया, और यह फ़िल्म उस शैली का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। मेघालय के आदिवासियों के बीच विवाह की अनोखी रीति और उसे चलाने वाले समाज से परिचय कराती, नन्दिनी बेदी की २००८ की फ़िल्म ‘नोट्स औन मैनकैप्चर’ भी इसी परम्परा में है।
वृत्त चित्रों की विरासत के रूप में यह जो समझ विकसित हुई थी कि डौक्यूमेण्टरी सिर्फ़ वस्तुगत सच्चाई का चित्रण भर है। इस पुरानी पड़ गई सोच के बरक्स नए डौक्यूमेण्टरी फ़िल्मकारों ने अपने लिए नए मुहावरे तलाशना शुरु कर दिया। मनोजगत के पहलुओं को भी यथार्थ के रूप में जगह देने के लिए नाट्य रूपान्तर, गानों, एनीमेशन, ग्राफ़िक्स सभी तत्वों के इस्तेमाल किया गया। कलारूपों की इस आज़ादी का परिणाम ये हुआ कि फ़िल्म में दिख रहे लोगों का ही नहीं, फ़िल्मकार का व्यक्तित्व भी फ़िल्म में झलकने लगा। क्योंकि वह स्वयं भी यथार्थ का एक हिस्सा है।
इस लिहाज़ से पारोमिता वोहरा की नारीवादी फ़िल्म ‘अनलिमिटेड गर्ल्स’ (२००२) बेहद अहम फ़िल्म है, क्योंकि उसने नारीवाद जैसे रूखे समझे जाने वाले विषय को एक ऐसे मनोरंजक स्वरूप में ढाला कि वह नई पीढ़ी के लिए सुस्वादु हो गया अपने विषय के साथ किसी तरह का समझौता किए बिना । इस्मत चुग़ताई और सआदत हसन मंटो के काल्पनिक वार्तालाप के गिर्द बुनी हुई मधुश्री दत्ता की फ़िल्म ‘सेवेन आईलैन्ड्स एण्ड ए मेट्रो’ (२००६) मुम्बई शहर के वस्तुनिष्ठ यथार्थ से अधिक मुम्बई शहर के उदास अन्तर्भाव पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है।
दूसरी ओर स्वयं फ़िल्मकार को केन्द्र में रखकर कहानी सुनाने का अन्दाज़ विकसित हुआ है क्योंकि निजी का वृहद स्तर की वास्तविकता से रिश्ता है, सूक्ष्म में विराट की झलक है।’ पंकज ऋषिकुमार की ‘कुमार टाकीज़’ एक छोटे कस्बे के एक बंद हो चुके सिनेमा हाल और उसके ज़रिये फ़िल्मकार के परिवार की एक निजी कथा कहती है। अजय रैना अपनी फ़िल्म ‘टैल देम द ट्री दे हैड प्लाण्टेड हैज़ नाउ ग्रोन’ (२००१) में कश्मीर घाटी स्थित अपनी पारिवारिक जड़ों को टटोलते हुए वहाँ लोगों के बदलते हुए मिज़ाज को पकड़ते हैं। और इस सब से इतर श्यामल करमाकर की ‘आई एम दि वेरी ब्यूटिफ़ुल’ (२००६) जैसी फ़िल्म है जो फ़िल्मकार के उसके विषय- एक प्रौढ़ होती बार सिंगर के सम्बन्ध को एक ख़तरनाक श्रृंगारिक धार पर बनाए रखती है और अपने दर्शक को वायेरिज़्म के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।
***
ये कुछ यादगार और पथप्रवर्तक फ़िल्में हैं। और इन में अधिकतर फ़िल्में निजी प्रयासों, किसी एन जी ओ की आर्थिक सहायता, या विदेशी अनुदान के सहारे बनी हैं। जबकि भारत में अधिकतर डौक्यूमेण्ट्री फ़िल्में दूरदर्शन के सहयोग से, मंत्रालयों के अनुदानों से बनती हैं। कम ही लोग होते हैं जो अपने तईं फ़िल्म का निर्माण करते हैं। पिछ्ले बीस साल में कुछ अच्छे बदलाव ज़रूर हुए हैं मगर अभी भी डौक्यूमेण्ट्री फ़िल्मों की न कोई समुचित अनुदानतंत्र विकसित हुआ है, न तो कोई वितरण व्यवस्था विकसित हो सकी है और न ही कोई पेशेवर संस्कृति बन पाई है। इस सूरते हाल पर अजय रैना मानते हैं कि इसकी मुख्य ज़िम्मेवारी सैटेलाइट चैनलों की है जो अपनी व्यापक पहुँच के बावजूद न तो वे स्वयं डौक्यूमेण्ट्री बनाते हैं, न उसके लिए अनुदान देते हैं और तो और दिखाते तक नहीं है।
भारत के डौक्यूमेण्ट्री मंज़र में इस बदलाव में सरकार और भारतीय बाज़ार की कोई विशेष भूमिका भले न हो मगर विस्व बाज़ार की एक बड़ी भूमिका है। मधुश्री मानती हैं कि ये जो तथाकथित डिजिटल क्रांति हुई है, इसमें फ़िल्मकारों ने कुछ नहीं किया- ये तो सोनी ने तय किया। उन्होने इस बाज़ार को बनाया है और हम इस बाज़ार के हिस्से हैं। हम सोच सकते हैं कि हमने एक नया सौन्दर्यबोध गढ़ा है मगर वह आत्मश्लाघा और अपना ही महिमामण्डन होगा। दरअसल हम सोनी जैसे कम्पनियों के द्वारा बनाए माल के उपभोक्ता हैं। इस तरह की तकनीक आधारित कला का चुनाव करके हम सत्तातंत्र से बाहर नहीं रह सकते। हम हैं क्योंकि सोनी आदि कम्पनियों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि बड़ी संख्या में लोग फ़िल्मकार का चोला पहनें।
इसी बात को एक दूसरी गहराई देते हुए कमल स्वरूप बताते हैं कि कला को जब तक बेचा न जाय वो कला के रूप में स्वीकार नहीं होती। कला के पीछे एक वैचारिक बल हो और उसकी सांस्कृतिक बिक्री की जाय, तभी कला, कला बनती है। एण्डी वारहोल के पीछे अमरीका का पूरा विज्ञापन उद्योग और मार्शल दुशौं जैसे कलाविचारक का बल लगा हुआ था तभी वारहोल को एक अनोखे कलाकार के रूप में प्रतिष्ठा मिल सकी। कला की क़दर और कला की समझ कोई जन्म से ले के नहीं पैदा होता, उसकी शिक्षा लेनी पड़ती है। कमल स्वरूप अपनी मातृ संस्था एफ़ टी आई आई पुणे की मिसाल से अपनी बात को साफ़ करते हैं कि शुरुआत में योरोप ने अपनी फ़िल्में और फ़िल्मों पर किताबें मुफ़्त में भेजी। किताबों को पढ़कर और फ़िल्मों को देख-देख कर संस्था के छात्रों में योरोपीय फ़िल्मों के लिए एक स्वाद पैदा हुआ और वे योरोपीय फ़िल्मों के लिए एक दर्शक वर्ग में बदल गए। अभी वे लोग, फ़िल्म एप्रीसिएशन कोर्स के ज़रिये और लोगों को इस कला की सराहना में शिक्षित करते हैं, और उन्हे दर्शक में बदलते हैं। आज भारत में डौक्यूमेण्ट्री का कोई दर्शकवर्ग नहीं है, इसलिए उनका दर्शकवर्ग भी तैयार किया जा रहा है; जगह-जगह जो मैस कौम कोर्सेस शुरु किए गए हैं, उनसे डौक्यूमेण्ट्री का नया दर्शकवर्ग तैयार हो के निकलेगा। कला अन्ततः एक माल है, उसे भी बेचना पड़ता है।
कमल स्वरूप यह भी कहते हैं कि सूचना और ज्ञान की परिभाषाएं पहले से ही पश्चिम में तय हो जाती हैं। और अधिकतर लोग योरोप में हो रहे काम की नक़ल कर रहे होते हैं क्योंकि अनुदान संस्थाएं योरोप में हैं और वे तय करती हैं कि क्या चलेगा और कया नहीं, क्या कला है और क्या नहीं। फ़िल्मोत्सव में मिलने वाली पुरुस्कार भी इन्ही योरोपीय वैचारिक मानदण्डों व कलात्मक मानदण्डों पर मिलते हैं। तो चाहे-अनचाहे हर फ़िल्मकार उन्ही मानदण्डों के अनुसार सोचने और करने लगता है क्योंकि जिस फ़िल्मकार विदेश में पुरस्कृत न हुआ हो, उस की इज़्ज़त नहीं होती।
ऐसा मालूम दे सकता है कि फ़ीचर फ़िल्मों के मुक़ाबले डौक्यूमेण्टरी फ़िल्मों में फ़िल्मकार अपनी बातों को कहने के लिए अधिक स्वतंत्र है। ये थोड़ा सही है लेकिन थोड़ा नहीं भी। उनके पास आधी आज़ादी है। अभी भी उनको अपनी तरह की फ़िल्में बनाने के लिए, विषयों की बन्दिश से इतर, अपने प्रस्तावित मसविदों को भी ऐसी भाषा में और ऐसे जुमलों से सजा कर लिखना होता है कि पैसे की थैली पकड़ने वाली मुट्ठी उसे अपनी ही बात समझ कर ढीली हो जाय।
***
हाल के बर्षों में जिस तरह से मोबाइल फोन और कम्प्यूटरों में कैमरों की गुणवत्ता में इजाफ़ा हुआ है, और छवियों के सम्पादन की सुविधाएं मुहय्या हुई हैं, उस से व्यापक जन तक फ़िल्म बनाने का माध्यम की पहुँच हो गई है। इस राह से खुलती नई सम्भावनाओं के बारे में पारोमित को नहीं लगता कि उस से कोई क्रांति होने वाली है।वे पूछती हैं कि ८० के दशक में जब वी एच एस था, मगर लोगों ने उस से क्या किया? शादी के वीडियो बनाए। पारोमिता मानती हैं कि डौक्यूमेण्ट्री चाहे जिस भी शैली में हो, उस का मक़सद विमर्श के नए आयाम खोलना है। उसका काम यथार्थ का चित्रण नहीं बल्कि यथार्थ के प्रति जवाबदेह होना है। और इसी वजह से वह हमेशा हाशिये पर ही रहने वाली है। इतना ज़रूर है कि वह ऐसे लोगों के लिए भी कला के दरवाज़े खोलेगी जो अभी तक उस से वंचित थे। टेक्नोलौजी का लोकतंत्रीकरण कला की पहुँच का भी लोकतंत्रीकरण कर देगा।
जबकि अजय रैना मानते हैं कि मोबाईल फोन और इन्टरनेट के आने से ये हुआ है कि डौक्यूमेण्ट्री की पहुँच एक व्यापक दर्शकवर्ग तक हो गई है। यूट्यूब जैसे वितरणमंच के आ जाने से डौक्यूमेण्ट्री का जो रूप हम अभी तक जानते आए हैं, उस में बदलाव आना निश्चित है। अब इस नए दर्शकवर्ग की पसन्द और समझ के अनुरुप नए कलारूप विकसित होंगे। हमारी भी ऐसी ही उम्मीद है!
***
महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटरी फिल्में
१. कमला बाई, १९९२; रीना मोहन
२. हमारा शहर/ बौम्बे अवर सिटी, १९८५; आनन्द पटवर्धन
३. सिद्धेश्वरी, १९८९; मणि कौल
४. सेवेन आईलैण्ड्स एण्ड ए मैट्रो, २००६; मधुश्री दत्ता
५. इण्डिया '६७, १९६८; एस. सुखदेव
६. ए नाइट औफ़ प्रौफेसी, २००२; अमर कँवर
७. अनलिमिटेड गर्ल्स, २००२, पारोमिता वोहरा
८. ब्रह्मा, विष्णु, शिव, १९९९; आर वी रमणी
९. हवा महल, २००४, विपिन विजय
१०. आई एम दि वेरी ब्यूटिफ़ुल, २००६, श्यामल कर्माकर
(फिल्मकार पारोमिता वोहरा, मधुश्री दत्ता, कमल स्वरूप और अजय रैना की पंसद के आधार पर)
***
कहां से मिलेंगी ये फिल्में
लगभग चार दशको के स्वतंत्र डौक्यूमेण्ट्री आन्दोलन के बावजूद भी फ़िल्मों की वितरण की समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका था जब फ़िल्मकार और दर्शक के बीच को सम्बन्ध को नियमित और सुगम बनाने के लिए गार्गी सेन और उनके साथियों ने अपने मैजिक लैनटर्न फ़ाउण्डेशन के तहत २००६ में अण्डर कन्स्ट्रक्शन नाम के एक वैकल्पिक व्यवस्था की नींव डाली। इन का मक़सद न केवल आम जनता के बीच डौक्यूमेण्ट्री का प्रसार है बल्कि एक ऐसे संग्रह को भी तैयार करना जिसके ज़रिये डौक्यूमेण्ट्री को फ़िक्शन फ़िल्मों के साये से बाहर निकलने में मदद हो सके और वो अपने लिए एक ऐसा दायरा बना सके जो न सिर्फ़ मुम्बईया फ़िल्मों से अलग हो बल्कि टेलेविज़न से भी।
इस प्रकार से संग्रहित फ़िल्मों का अण्डर कन्स्स्ट्रक्शन और मैजिक लैनटर्न फ़ाउण्डेशन २००८ से विभिन्न शहरों में नए मिज़ाज और अन्दाज़ से फ़िल्मोत्सव कर रहे हैं। १०० से भी अधिक फ़िल्मकारों की तक़रीबन २५० महत्वपूर्ण फ़िल्मों का वितरण कर रहा है अण्डर कन्स्ट्रक्शन। इंटरनेट पर इन के वेब पते पर फ़िल्मों व फ़िल्मकारों की जानकारी प्राप्त भी की जा सकती है और फ़िल्में ख़रीदने की मालूमात भी हासिल की जा सकती है।
वेब पता: underconstruction@magiclanternfoundation.org
डाक पता: द्वारा मैजिक लैनटर्न फ़ाउण्डेशन
जे-१८८१, चित्तोरंजन पार्क, बेसमेण्ट
नई दिल्ली ११००१९
फोन: (०११) २६२७३२४४, ४१६०५२३९
(यह लेख दैनिक भास्कर की रविवारीय पत्रिका 'रसरंग' के लिए लिखा गया जो २५ जुलाई को सम्पादित रूप में प्रकाशित हुआ। यह असम्पादित रूप है।)
(यह लेख दैनिक भास्कर की रविवारीय पत्रिका 'रसरंग' के लिए लिखा गया जो २५ जुलाई को सम्पादित रूप में प्रकाशित हुआ। यह असम्पादित रूप है।)




10 टिप्पणियां:
ज्ञानवर्धक पठनीय निबन्ध
There are many other more documentary films which were made in India. here are some...
1. Father, son and the Holy war
2. War and peace
3. Bar girls
4. Khush
5. a track to Rudrprayg
6. The Shape of Water
"फ़िल्म आस्वाद"-- यह विषय पढ़ाई में जोड़ने की बात जयप्रकाश चौकसे ने काफ़ी बार उठाई है, जितने सालों से उन्हें पढ़ा रहा हूँ। इस बारे में उनकी पिछली ख़बर।
यह लेख रसरंग में पढ़ा था अच्छा लगा | इस बार आपने भी (अगले लेख में ) youtube की शक्ति का प्रयोग किया है, वो इस लेख से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है | बहुत अच्छा | डॉक्युमेंट्रीज के शोकीनों के लिए मैंने पूर्व में भी कुछ लिंक कमेन्ट में दिए थे आज फिर दिया जाना प्रासंगिक हो रहा है, परन्तु यहाँ आभासी जगत में मुझे अभी भी हिंदी डॉक्युमेंट्रीज के लिंक इतने उपलब्ध नहीं हुए हैं | पाठकों से अनुरोध है की यदि उनके पास आनंद पटवर्धन की डॉक्युमेंट्रीज के कोई लिंक हो तो जरूर बताएं |
http://www.documentary-area.blogspot.com/
http://www.blogcatalog.com/explore/free+documentary+download/
http://www.rajshri.com/Listing/Documentaries/Free-Hindi-Documentary-Films-Online
"भारत एक खोज" के कुछ episode यहाँ से देखे जा सकते हैं |
http://watchbharatekkhoj.blogspot.com/
Some more better links for documentaries,
http://freedocumentaries.org/index.php
http://www.rajshri.com/Listing/Documentaries/Free-Hindi-Documentary-Films-Online
http://www.blogcatalog.com/explore/hindi+documentary/
http://www.cultureunplugged.com/filmedia/index.php
http://www.documentary-area.blogspot.com/
http://documentaryheaven.com/
http://topdocumentaryfilms.com/
http://www.documentary-film.net/
http://www.snagfilms.com/
http://www.hbo.com/documentaries/index.html#
http://www.documentary24.com/
http://freedocumentaries.org/
http://www.indiemoviesonline.com/documentary
http://www.ovguide.com/movies-documentary.html
http://www.documentary-log.com/
http://www.surfthechannel.com/cat/61482/a.html
http://video.pbs.org/
http://www.guba.com/browse?category=Documentary
http://www.docu-view.com/list/all
http://www.moviesfoundonline.com/documentaries.php
http://www.babelgum.com/browser.php#grid%7CSEARCH,channelID:179910,hint_no_featured:1,order:ALPHABETICAL
http://www.documentarywire.com/
http://filmtalks.net/
Priy Abhay,
tumahara lekh poora pada isliye bhi ki pichle 6 saalon se poori tarah isi dunia mein rama hoon. Lekh achcha hai lekin adhoora bhi jaise ki isme Orissa mein chal rahe rajnetik ghamasaan aur uske baraks pratirodh kee avaaj ko uthane wale 2 mahavapoorna samoohon ka koi jikra nahi. Ve samooh hain Bhubneshwar ka Samdrishti jo har mahine Madhyantar naam se video magazine niklata hai aur Bhavanipatanam ke yuva patrakaaron ka samooh KBK Samachaar (Kalahandi-Bolangir-Koraput Samachaar). Ye samooh ek nai bhasha ke saath saath bina funding ke apni jameen par majbooti se khare hain.Inhi do samoohon kee vajah se Niyamgiri pahadiyon ke vinaash kee khabarain Vedanta jaise bare multinational ke laakh na chaane ke baavjood saari dunia ke saamne aa saki hain. Iske alava dher saare chote film samarooh jo Magic Lantern Foundation kee tarah kisi Ford Foundation se nahi balki apne logon kee madad se viksit ho rahe hain aur ve bhi ek samanantar distribution network taiyyar kar rahe hain. Jiski andekhi bare media gharaane to kar hi rahe hain lekin tumahre jaise avayvsayaik blog mein jikra bhi na aaye to kisi design ka andesha hota hai.
Sanjay Joshi
Convener, Gorakhpur Film Festival
प्रिय संजय, तुमने अपना बहुमूल्य समय इस लेख को दिया इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जिन दो समूहों की चर्चा तुमने की है, उनकी जानकारी मुझे नहीं थी। तुमने उनकी चर्चा यहाँ कर के अच्छा किया।
मैं अपने बचाव में सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि मेरी जानकारियाँ सीमित हैं। फिर इस लेख की ज़मीन ९० के बाद आए डौक्यूमेण्टरी के स्वभाव में आए बदलाव को रेखांकित करना था। राजनीतिक प्रतिरोध के सिनेमा की चर्चा मैंने की है और जिस में आनन्द पटवर्धन और संजय काक जैसे फ़िल्मकारों का ज़िक़्र भी है। उड़ीसा के जिन दो समूहों की चर्चा कर मैं ज़रूर सकता था, यदि मेरा उद्देश्य वर्तमान दौर में चल रहे प्रतिरोध के सिनेमा को रेखांकित करना होता। मेरा मक़्सद महज़ प्रवृत्तियों को पकड़ना था।
एक समान्तर फ़िल्मोत्सव के अस्तित्व से मैं वाकि़फ़ हूँ जो आप चलाते हैं। लेकिन वह डौक्यूमेण्ट्री फ़िल्मों के वितरण का कोई विकल्प भी बन रहा है यह जानकारी मुझे नहीं है। यदि ऐसा है तो आप अपने जवाब में उस के बाबत विस्तार से लिखें.. स्वागत है!
Some very acclaimed and interesting Documentary Films are being distributed by Syncline filmstore (www.synclinefilmstore.com) They are the official distributor for films commissioned and produced by Public Service Broadcasting Trust (PSBT) www.psbt.org
अभय जी,
आपके इस लेख का लिंक Film writers association के ब्लॉग पेज में साईड बार में दे रहा हूँ :)
उम्मीद है कुछ और फिल्म प्रेमी इस जानकारीप्रद लेख का आनंद उठायेंगे।
http://www.fwa.co.in/FWABLOG/default.aspx
एक टिप्पणी भेजें